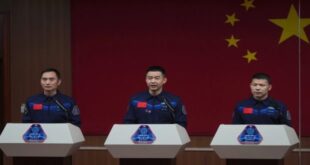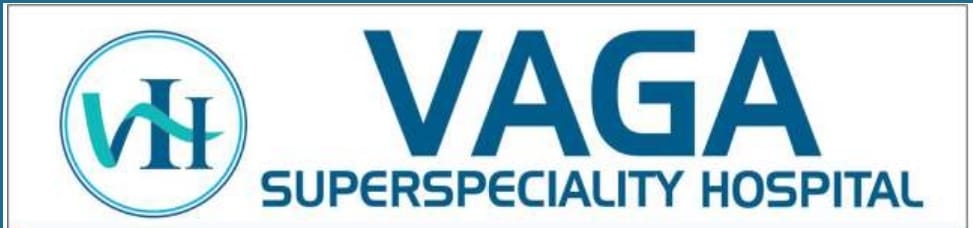हाल ही में संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा उद्देशिका से ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्दों को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें दावा किया गया है कि यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है, जिसकी व्याख्या 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में देश के शीर्ष न्यायालय द्वारा की गई थी। मूल ढांचे का सिद्धांत संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति पर एक सीमा निर्धारित करता है।
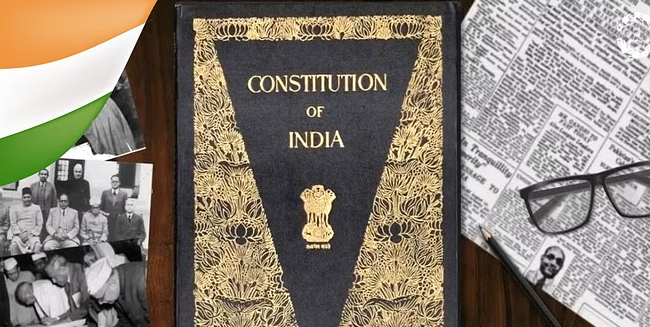
इसमें कहा गया है कि संसद उन मूल्यों को परिवर्तित या विकृत या संशोधित नहीं कर सकती है, जिनसे इस ढांचे का निर्माण हुआ है। यह सिद्धांत इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि यह नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके अधिकार और राज्य के प्राधिकार के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे भारत में संविधानवादी विचारधारा की रक्षा होती है। हालांकि न्यायालय ने इन याचिकाओं पर सुनवाई अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है।
उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल से ही भारत अपने चरित्र और भावना, दोनों में सहिष्णु और पंथनिरपेक्ष रहा है और अपने बहुरूपदर्शक सांस्कृतिक परिदृश्य की दृढ़ता से रक्षा करता रहा है। इसी प्रकार वर्षों से समाज में मौजूद विषमताओं के आलोक में समता आधारित सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। हालांकि, उदार लोकतांत्रिक मानसिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही है,
जिसने एक जीवंत लोकतंत्र की नींव रखी है। यही कारण है कि संविधान में ऐसी सभी विचारधाराओं को शामिल किया गया है, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि राष्ट्र विविधता में एकता के अंतर्निहित सिद्धांत के साथ एकीकृत और अखंड बना रहे।
इस पृष्ठभूमि में, सबसे पहले मूल संविधान में निहित प्रावधानों पर एक नजर डालना अनिवार्य है। भारत ने उदारवाद के विचार पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है और वितरणात्मक न्याय प्रदान करने के लिए समतावादी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। संविधान निर्माताओं ने इन विचारधाराओं को बहुत बुद्धिमत्ता से संतुलित किया था और इसी कारण उद्देशिका में न तो उदारवादी और न ही समाजवादी शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग किया था। उदार लोकतंत्र के विचार को भाग III (अनुच्छेद 14-32) में निहित मौलिक अधिकारों में संस्थागत रूप दिया गया है,
जबकि समतावादी विचार की जड़ें भाग IV में राज्य नीति-निर्देशक तत्वों के रूप में रखी गई हैं, जो वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत को स्थापित करती हैं। इसका अर्थ संसाधनों का समतामूलक वितरण (आवश्यकताओं के अनुसार) करना है और इसकी व्याख्या अनुच्छेद 38, 39 और 46 में की गई है।
 Samar Saleel Samar Saleel News Portal
Samar Saleel Samar Saleel News Portal