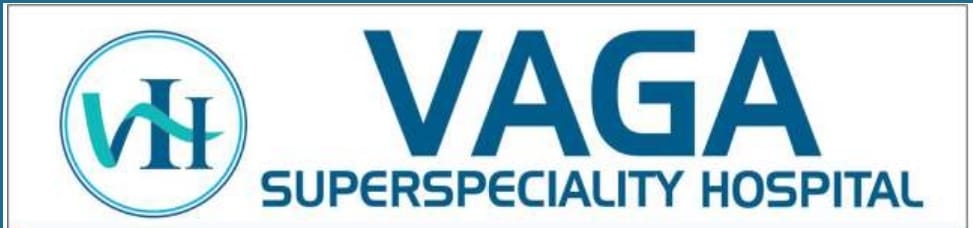भारत जैसे विशाल और विविध देश में, संसद के लोकप्रिय सदन और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव राजनीतिक गतिशीलता और एक अद्भुत पैमाने की संगठनात्मक जटिलताओं से जुड़े कार्यक्रम हैं। ये चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के चुनाव प्रणाली का उपयोग करके किए जाते हैं और एक साधारण बहुमत के आधार पर तय किए जाते हैं। विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। चूंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का एक गैर-प्रश्न है, इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि चुनावों को इस तरह से प्रबंधित किया जाता है जो अधिक प्रतिनिधि संसद / राज्य विधानसभाओं को बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करता है। ऐसे चुनावों की समय-सीमा ज्ञात करना आसान नहीं है।

चुनाव आयोग, जो चुनावों के लिए समय निर्धारित करता है, को मौसम की स्थिति को ध्यान में रखना पड़ता है – सर्दियों के मौसम के दौरान, निर्वाचन क्षेत्र बर्फ से बंधे हो सकते हैं और मानसून के दौरान, दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच मुश्किल और प्रतिबंधित हो सकती है; कृषि चक्र ताकि फसलों का रोपण या कटाई बाधित न हो; परीक्षा कार्यक्रम- जैसे कि मतदान केंद्रों के रूप में स्कूलों का उपयोग किया जाता है और शिक्षकों को चुनाव कर्तव्यों के लिए तैनात किया जाता है; धार्मिक त्यौहार और सार्वजनिक अवकाश इत्यादि, इसके ऊपर, लॉजिस्टिक कठिनाइयाँ हैं जो इस तरह के चुनाव कराने के साथ होती हैं-मतपेटियों या ईवीएम को बाहर भेजना, मतदान केंद्रों की स्थापना करना, चुनावों की देखरेख के लिए अधिकारियों की भर्ती करना, इत्यादि। संसद के लोकप्रिय सदन (लोकसभा) के गठन के लिए भारत में आम चुनावों में व्यापक रूप से भिन्न भौगोलिक और जलवायु क्षेत्रों में फैले लगभग 7,00,000 मतदान केंद्रों में लगभग 700 मिलियन मतदाताओं के साथ दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का प्रबंधन शामिल है। हिमालय में बर्फ से ढके पहाड़ों, राजस्थान के रेगिस्तानों और हिंद महासागर में काफी आबादी वाले द्वीपों में स्थित मतदान केंद्र हैं। आम चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को 4 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देना पड़ता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शांतिपूर्ण और स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हों, बड़ी संख्या में नागरिक और पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों को तैनात किया जाना है।
यह बताना गलत नहीं होगा कि भारतीय राजनीति हमेशा एक चुनावी मोड में होती है। अब तक, लोकसभा के सामान्य 5 साल के कार्यकाल में कुछ असाधारण वर्षों को छोड़कर, हर साल औसतन 5-7 राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जब राज्य की विधानसभाओं के चुनाव अन्य राज्य विधानसभाओं के चुनाव के एक महीने के भीतर घोषित किए जाते हैं। इस तरह के अक्सर चुनावी चक्रों में न केवल वित्तीय और अन्य संसाधन निहितार्थ होते हैं, बल्कि राज्यों के साथ-साथ देश में भी प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियों में बाधा आती है और सामान्य रूप से शासन प्रक्रिया को संकट में डालती है। सरकारें और राजनीतिक दल कभी न खत्म होने वाले प्रचार मोड में बने रहते हैं और चुनावी मजबूरियाँ ध्यान केंद्रित करती हैं।

विभिन्न स्तरों पर एक साथ चुनावों के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। एक साथ चुनाव कराना आदर्श रूप से यह दर्शाता है कि संवैधानिक संस्थानों के सभी तीन स्तरों पर चुनाव एक समन्वित और समन्वित रूप से आयोजित किए जाते हैं। इसका प्रभावी रूप से मतलब यह है कि एक मतदाता एक ही दिन में सरकार के सभी स्तरों के लिए निर्वाचित सदस्यों के लिए अपना वोट डालता है। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि शासन के सभी स्तरों पर समवर्ती चुनाव आयोजित करना अस्थिर और व्यावहारिक रूप से असंभव है। तृतीय श्रेणी संस्थान, अर्थात नगरपालिका और पंचायत, मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य विषय हैं।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों द्वारा तृतीय श्रेणी के संस्थानों के चुनावों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है और देश में इनकी संख्या काफी बड़ी है, इसलिए लोकसभा के साथ तीसरे स्तर पर चुनाव कार्यक्रम को सिंक्रनाइज़ करना और संरेखित करना असंभव और असंभव होगा। और राज्य विधानसभा चुनाव। यह मामला होने के नाते, लोकसभा और विधान सभाओं के लिए एक साथ बदलाव करने की व्यवहार्यता को एक गंभीर सोच दी जा रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि एक साथ चुनाव न केवल मतदाताओं के उत्साह को जीवित रखेंगे, बल्कि सरकारी खजाने को भारी बचत भी देंगे। यह माना जाता है कि दोहराए जाने वाले प्रशासनिक व्यस्तता से भी बचा जा सकता है, यह भी महसूस किया गया है कि अनुकरणीय चुनाव राजनीतिक दलों के खर्चों को नियंत्रित करेंगे और आदर्श आचार संहिता के बार-बार लागू होने से बचेंगे जो सरकार द्वारा विकासात्मक और कल्याणकारी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं।

एक साथ चुनाव के पक्ष में कई सम्मोहक कारण हैं। विकास कार्यक्रमों का निलंबन, आदर्श आचार संहिता के बार-बार लागू होने के कारण कल्याणकारी गतिविधियाँ, सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर व्यय और लगातार चुनावों पर विभिन्न हितधारकों, काले धन, एक लंबे समय के लिए सरकारी कर्मियों और सुरक्षा बलों की व्यस्तता, जाति, धर्म का नाश और सांप्रदायिक मुद्दे आदि, शासन और नीति निर्माण पर लगातार चुनावों का प्रभाव शायद सबसे महत्वपूर्ण है। बार-बार चुनाव सरकारों और राजनीतिक दलों को स्थायी “अभियान” मोड में रहने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे नीति निर्माण का ध्यान केंद्रित होता है। अल्प-दृष्टि वाले लोकलुभावन और “राजनीतिक रूप से सुरक्षित” उपायों को “कठिन” संरचनात्मक सुधारों पर उच्च प्राथमिकता दी जाती है, जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण से जनता के लिए अधिक फायदेमंद हो सकते हैं। यह उप-इष्टतम प्रशासन की ओर जाता है और सार्वजनिक नीतियों और विकासात्मक उपायों के डिजाइन और वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
भारत के माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधान मंत्री ने सार्वजनिक मंचों पर एक साथ चुनाव कराने के लिए अपना समर्थन देने के लिए समय दिया है। माननीय प्रधान मंत्री ने बताया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के अलावा, देश भर में चुनावों का एक निरंतर चक्र एक बड़ी लागत के अलावा आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण काम करता है। माननीय प्रधान मंत्री ने नेताओं से इस मामले पर बहस शुरू करने और प्रस्ताव के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करने के लिए भी कहा है।
29 जनवरी 2018 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए अपने संबोधन में, भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने कहा था कि “देश में शासन की स्थिति के लिए जीवित नागरिक लगातार चुनावों के बारे में चिंतित हैं” देश का एक हिस्सा या दूसरा, जो अर्थव्यवस्था और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बार-बार चुनाव न केवल मानव संसाधनों पर भारी बोझ डालते हैं, बल्कि आदर्श आचार संहिता के प्रचार के कारण विकास प्रक्रिया को बाधित करते हैं। इसलिए, एक साथ चुनाव के विषय पर एक निरंतर बहस की आवश्यकता है और सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने की आवश्यकता है।

पहले के अवसर पर, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने यह देखा था कि “वर्ष भर कुछ चुनाव या दूसरे के साथ, सरकार की सामान्य गतिविधियाँ आचार संहिता के कारण स्थिर रहती हैं। यह एक विचार है जिसे राजनीतिक नेतृत्व को सोचना चाहिए। यदि राजनीतिक दल सामूहिक रूप से सोचते हैं, तो हम इसे बदल सकते हैं। चुनाव आयोग भी अपने विचार और प्रयासों को एक साथ चुनाव कराने में लगा सकता है और यह अत्यधिक लाभकारी होगा ”।
संविधान और विषय वस्तु विशेषज्ञों, थिंक टैंक, सरकारी अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करने वाले हितधारकों के एक केंद्रित समूह को एक साथ आने और उचित कार्यान्वयन से संबंधित विवरणों पर काम करने की आवश्यकता है। इसमें उपयुक्त संविधान और वैधानिक संशोधन शामिल हो सकते हैं, एक साथ चुनावों के लिए संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यावहारिक ढांचे पर सहमति, एक हितधारक संचार योजना विकसित करना आदि।

सलिल सरोज
 Samar Saleel Samar Saleel News Portal
Samar Saleel Samar Saleel News Portal